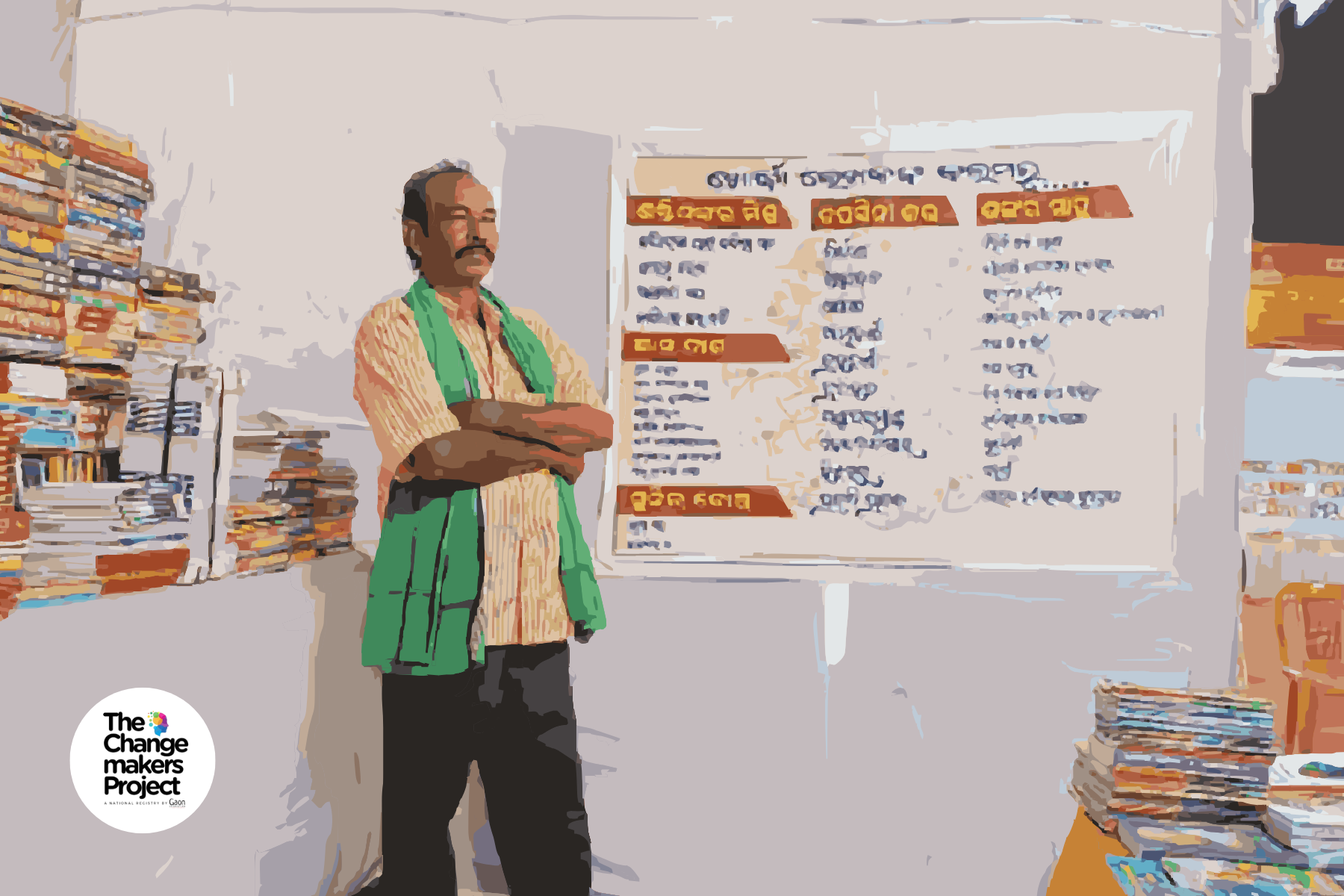हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार में सुनते हैं, कि अमेरिका में अमुक संस्था के छात्रों ने अपने ही सहपाठियों को गोली से उड़ा दिया। इस प्रकार की उद्दंडता और अपराधी मानसिकता के लिए शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार होती है, इसके बिपरीत हमारे देश में अध्यापक स्वयं अनुशासित और समाज के लिए समर्पित हुआ करते थे, जिसके फलस्वरूप ‘अरुणी उद्दालक’ जैसे आज्ञाकारी छात्र तैयार होते थे। अब हमारे यहाँ भी पश्चिमी शिक्षा पद्धति का बोलबाला हो गया है और विद्या केवल किताबों के प्रश्नों में दब कर रह गयी है। हमारे समाज को यदि अनुशासित और समर्पित छात्र चाहिए तो हमें अपनी परम्परा को और अध्यापकों को पूर्ण समर्पण भाव लेकर चलना होगा।
40 के दशक में शिक्षा के लिए स्कूल तो बहुत कम थे, लेकिन आज की अपेक्षा में गुणवत्ता अधिक थी, इसके विपरीत आजादी के बाद स्कूलों की संख्या बढ़ती गई है, लेकिन उसी के हिसाब से शिक्षा की गुणवत्ता घटती चली गई है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पक्के स्कूल बने हैं और बड़ी संख्या में अध्यापक मौजूद हैं और वह मोटी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। गाँव का मामूली आदमी परिषदीय विद्यालयों में भेजना नहीं चाहता। प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पर फीस भी अधिक है जो गाँव के लोगों की सामर्थ्य के बाहर है। जब प्राइमरी शिक्षा ही लचर हो जाती है, तो बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते तो वह अपना भविष्य निर्धारण कैसे कर पाएंगे।
पुराने समय में गाँवों में अंग्रेजी और अनेक अन्य विषय तो नहीं पढ़ाये जाते थे, लेकिन निकलने वाले बच्चों की हिन्दी और गणित बहुत मजबूत होती थी। अब अंग्रेजी माध्यम के नाम से तमाम स्कूल खुले हैं ,जहाँ पर अंग्रेजी कहने को तो पढ़ाई जाती है, लेकिन हिन्दी भी ठीक प्रकार से ना लिख पाते हैं ना पढ़ पाते हैं। अध्यापकों में वह पुराना कर्तव्य बोध बिल्कुल नहीं बचा है। ग्रामीण स्कूलों से निकले हुए ऐसे छात्र जब माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं में जाते हैं, तो उनकी नींव कमजोर होने के कारण वे चल नहीं पाते, अकसर कई छात्र पढ़ाई छोड़ भी देते हैं , इसलिए ग्रामीण छात्रों में ड्रॉप आउट की संख्या बहुत अधिक है।

यह छात्र ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ अकसर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता और स्कूलों में पढ़ाई ठीक से होती नहीं, परिणाम स्वरूप वह आगे चल नहीं पाते, तो बेरोजगारी का शिकार बनते हैं। जो बच्चे मेहनत करके पढ़ भी जाते हैं, वह हाई स्कूल, इण्टर, बी.ए. और एम.ए. पास करते चले जाते हैं, लेकिन किसी स्तर पर जीवन यापन के लिए अपना रास्ता नहीं चुन पाते और अगर रास्ते की जानकारी भी है तो उस पर चल नहीं पाते, अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। रोजगार परक शिक्षा की बातें तो बहुत होती हैं और इस के लिए नियमित शिक्षण संस्थान भी खोले गए हैं, लेकिन वह रोजगार दिलाने का माध्यम नहीं बन पाए, यहां तक कि इंजीनियर और डॉक्टर भी अपना व्यवसाय तो आरम्भ नहीं कर सकते, सरकारी नौकरियां ढूंढते हैं, जो मिल नहीं पाती।
उच्च शिक्षा की संस्थाओं में भीड़ बहुत है, लेकिन वहाँ से निकले हुए छात्रों के लिए रोजगार या नौकरी नहीं है। ऐसी हालत में उच्च शिक्षा में केवल मेधावी छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिए और प्रजातन्त्र के नाम से सबको उच्च शिक्षा का अधिकारी नहीं मानना चाहिए तब ऊपर के स्तर पर बेरोजगारी घटेगी। हम मैकाले के अनुसार पढ़े लिखे लोग तैयार कर रहे हैं, जिसने कहा था ‘वी हैव टू प्रोड्यूस क्लर्क’। सही माने में बी.ए. करने वाले लोग अच्छे क्लर्क भी नहीं हो सकते, तब उन्हें कैसे नौकरी मिलेगी।
गाँव की अपेक्षा शहरों के विद्यालय कुछ बेहतर होते हैं, लेकिन वहाँ भी बड़े नेताओं, अधिकारियों और धनवानों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। सम्पन्न लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए देश के बाहर भेज देते हैं और जो नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले लोग हैं , उन्हें ग्रामीण स्कूलों या ग्रामीण शिक्षा की कोई जानकारी तथा चिन्ता नहीं, क्योंकि उनके बच्चे तो वहाँ पड़ेंगे नहीं। पुराने समय में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर बड़ी संख्या में होते थे, अध्यापकों पर विशेष कर सरकारी अध्यापकों पर दबाव बना रहता था और वह काम करते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है।
यदि निरीक्षकों की भर्ती नहीं हो सकती तो समाज को निगरानी करने का मौका देना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम की भूमिका का विस्तार करके प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी पंचायत को दे दी जाए, तब शायद बेहतर निगरानी हो सकेगी। क्योंकि गाँव में साक्षरता की आज भी बहुत कमी है, इसलिए बच्चों का होमवर्क घरों में कराया नहीं जा सकता। समस्या काफी हद तक हल हो सकती है, यदि सरकार खैरात बाँटने के बजाय गाँव में अच्छे स्तर के आवासीय विद्यालय खोलकर और मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए।

गाँव में अच्छे कारीगर ढूंढने से भी नहीं मिलते जैसे बढ़ाई, लोहार, थवाई यानी मकान बनाने वाले, बिजली ठीक करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और यहाँ तक कि अच्छे दर्जी नहीं मिलते, उनके पास रोजगार की कमी नहीं है और वह बेरोजगार नहीं हो सकते। इस समस्या के समाधान के लिए जो आईटी कॉलेज या स्कूल खोले जाते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल शिक्षा शायद कम रहती हो या फिर वहाँ से निकले हुए छात्र गाँवों में काम नहीं करना चाहते, शहर जाना और शहर में काम से जुड़ना यह हर बार सम्भव नहीं हो पाता। अक्सर पढ़े लिखे लोग हाथों से काम नहीं करना चाहते और बुद्धिजीवी भी बनने के लिए उनमें एक क्षमता नहीं है, श्रमजीवी कभी भी बेरोजगार नहीं होता, इसलिए उच्च शिक्षा में भीड़ घटाने की आवश्यकता है छोटे स्तर पर रोजगार परक शिक्षा देकर उन्हें रोजगार प्रेरित स्वभाव पैदा करना चाहिए।
पुराने समय में गाँव अपने में पूर्ण होते थे और लगभग प्रत्येक गाँव में या पास पड़ोस में कारपेन्टर, लोहार, जुलाहे रहते थे, जो स्थानीय आवश्यकता के लिए चीजों की आपूर्ति करते थे। अब यह सब शहर को चले गए, भले ही वहाँ जीवन सुखी नहीं है खान-पान उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन दूसरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शहर जाने का फैसला किया। कष्ट की बात यह है कि यह व्यावसायिक समूह जातियों के रूप में आ गए और उनमें ऊच-नीच की भावना पैदा कर दी गई, यही से हमारे समाज का विघटन और विभाजन शुरू हुआ होगा।
अब हालात यह है कि सोलर पैनल गाँव-गाँव में लगवाए तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए उनको मेन्टेन करने के लिए ध्यान रखने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे ही बिजली की पूर्ति गाँव-गाँव तक हुई है लेकिन इलेक्ट्रीशियन नहीं है और इन्हें पैदा करने के लिए कोई संस्थान भी नहीं है, इसलिए आवश्यकता यह है, कि उनके सीखने के बाद रोजगार की गारन्टी हो, तभी इन तमाम आधुनिक व्यवसायों में नवयुवक और नवयुवतियाँ जाएगी, अन्यथा पैनल लगाने भर से बिजली पहुंचने से पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। एक तरफ आईटी शिक्षण संस्थान बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ समाज उपयोगी व्यवसाय में काम करने के लिए कारीगर तैयार नहीं किया जा रहे इसे दुर्भाग्य ना कहें तो क्या कहें।
एक तरफ गाँव में तकनीकी ज्ञान वाले लोग उपलब्ध नहीं है, तो दूसरी तरफ शहरों में इनकी बेरोजगार फौज मौजूद है, क्योंकि गाँव में यह रहना नहीं चाहते। देश की क्या आवश्यकता होने वाली है अगले 5 वर्ष में कितने डॉक्टर इंजीनियर और विशेषज्ञ चाहिए उसके हिसाब से शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा खोले जाएं, तो कुछ आसानी होगी विशेष कर यदि ऐसे संस्थान गाँव में खोले जाएं, तब शायद यह समस्या हल हो सकती है। जब इन विशेषज्ञों को और तकनीकी ज्ञान वालों को देश में रोजगार नहीं मिल पाता तब वह विदेश की राह पकड़ते हैं और देश का प्रतिभा पलायन होता है, ‘ब्रेन ड्रेन’ होता है और विदेशियों को बिना कुछ खर्च किए विशेषज्ञ मिल जाते हैं, भारत के खर्चे पर , क्योंकि इन विशेषज्ञों को तैयार करने में जो शिक्षा संस्थान चलाए जाते हैं, उन पर सरकार का बहुत बड़ा खर्च होता है और जनता पर उसका बोझ आता है।
शिक्षा पर निरन्तर नजर रखने की आवश्यकता होगी और शिक्षित बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, इसका कारण भी खोजना होगा, अन्यथा बेरोजगारी बढ़ती जाएगी हम बिना सोचे समझे शिक्षण संस्थान खोलते जाएंगे और बिना लक्ष्य, विशेषज्ञों की और काफी पढ़े-लिखे लोगों की फौज, जिसके लिए काम नहीं है वह तैयार होगी। सोचने का काम प्राइवेट संस्थान या उन्हें खोलने वाले धनाढ्य लोग नहीं करेंगे, यह काम सरकार को ही करना होगा और आवश्यकता अनुसार ही ऐसे लोग तैयार करने होंगे, जिन्हें आराम से रोजगार मिल सके और 70% आबादी वाले देश के गाँव के हिस्से में उसी अनुपात में शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए, उनका शहरों में जमावड़ा रोक पाना सरकार के लिए मुश्किल नहीं है।
कष्ट की बात है, कि योजना आयोग जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया, बजाय इसके उसमें परिवर्तन करना चाहिए था, ताकि वह पंचवर्षीय योजनाओं के लिए समुचित तैयारी करवा सकता, अब उसकी जगह पर नीति निर्धारण करने के लिए नीति आयोग तो है लेकिन वह कितना प्रभावी हो रहा है कहना कठिन है।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भवन और फर्नीचर की अपेक्षा अध्यापकों की अधिक आवश्यकता है। अध्यापकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरा नहीं जाता और लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत ही नहीं हो रहे हैं, जो पद रिक्त हो रहे हैं उन्हें भी भरा नहीं जाता, बल्कि आउटसोर्सिंग के द्वारा भरने की बात कही जाती है। हमारे देश में कहा जाता है कि ‘बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे’ तो स्वाभाविक है कि जब गुरुओं के स्थान ही रिक्त पड़े हैं तो ज्ञान कौन देगा? शिक्षा को सार्थक कैसे बनाया जा सकेगा? यह विचारणीय प्रश्न है।