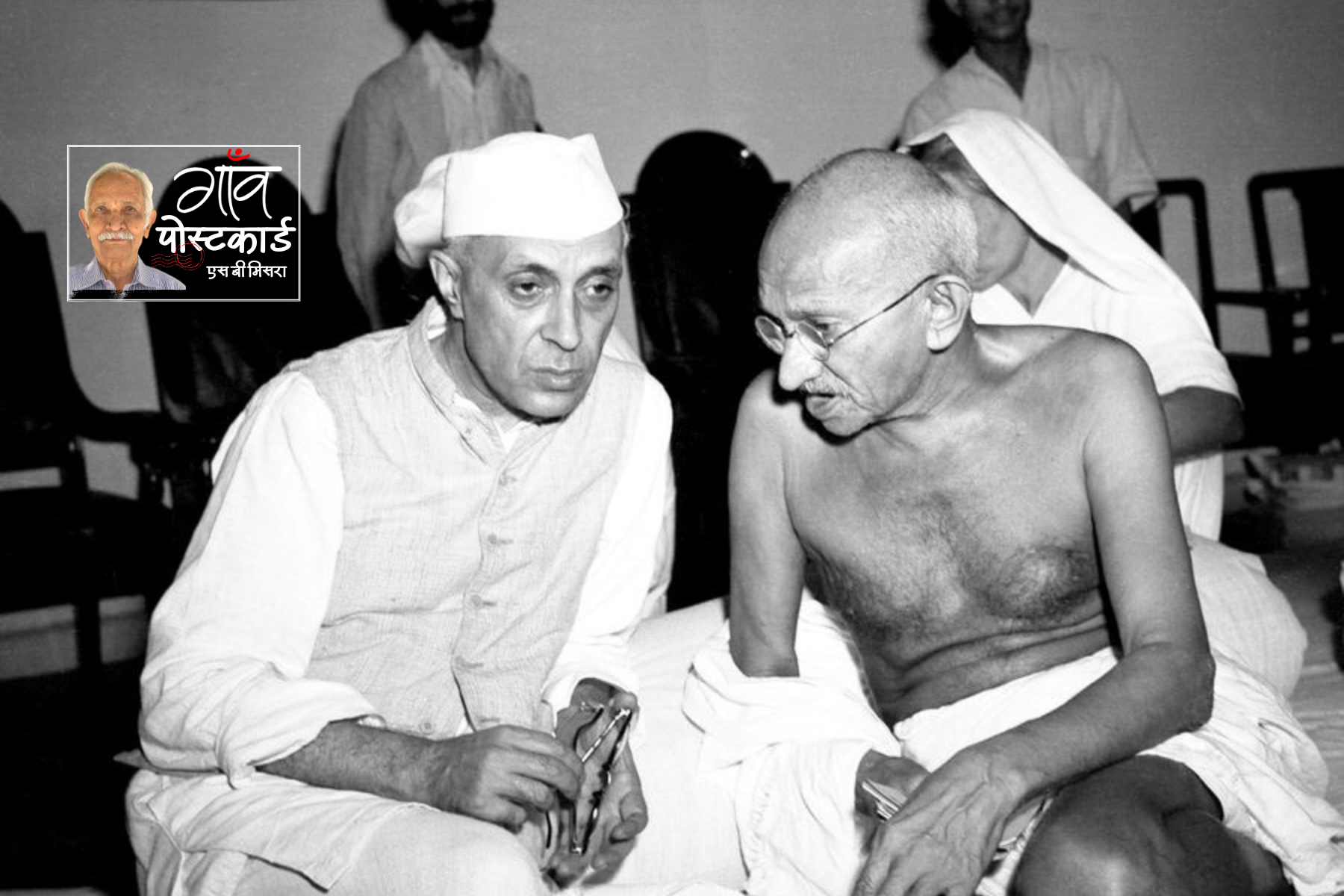गाँव कनेक्शन: आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तो जैसे संवाद में इतने साल की यात्रा पूरी कर ली है तो हमारे दर्शकों, श्रोताओं को जानना है की संवाद क्या है?
सौरव रॉय: शुक्रिया। यह बहुत कठिन सवाल नहीं है। संवाद, संवाद ही है – एक संवाद की प्रक्रिया, जो हमें लगता है कि कम होती जा रही है और जिसकी आज और अधिक आवश्यकता है। संवाद, जैसा कि आपने कहा, यह 11वां संस्करण है, लेकिन लगभग 10 साल हो चुके हैं। यह 2014 में शुरू हुआ था। हम एक मंच बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ सांस्कृतिक उत्सवों पर बातचीत हो सके, और भारत की विभिन्न आदिवासी समुदायों से लोग आकर चर्चा करें, मिलें और देखते हैं कि इससे क्या निकलता है। इसी तरह इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे-धीरे हमने संवाद में हर साल किसी एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित किया – जैसे एक साल भाषाओं पर, एक साल आदिवासी चिकित्सा पर, एक साल खेल पर। इस तरह से 4-5 सालों में हमें एक दिशा मिली। तब तक संवाद भी एक इको-सिस्टम बन चुका था, जिसके साथ हम संघर्ष कर रहे थे। 2018-19 तक आते-आते, आज संवाद एक वार्षिक मंच बन गया है। नवंबर 15 से 19 तक जमशेदपुर में हर साल लगभग 25,000 से 30,000 लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार भी 25,000 से अधिक लोग यहाँ आए हैं। ये सभी साथी अपनी कहानियाँ, महत्वाकांक्षाएँ और भरोसा लेकर आते हैं। 180 आदिवासी समुदायों, 24 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से लोग हिस्सा लेते हैं। यहाँ चर्चाएँ होती हैं, उत्सव मनाए जाते हैं।

इसके साथ ही हम हर साल लगभग 20 से 25 क्षेत्रीय संस्करण भी आयोजित करते हैं, जहाँ हम उनके समाज और परिस्थितियों में जाकर संवाद करते हैं। यह संवाद का पहला हिस्सा है। इसके बाद कई एक्शन रिसर्च प्रोग्राम भी होते हैं। भाषाओं पर करीब 11 आदिवासी भाषाओं के साथ काम हो रहा है, जिसमें शिक्षण सामग्री तैयार करना, संगीत, चिकित्सा, कला, खेल और धरोहर के तत्व शामिल हैं। इस पूरे प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आदिवासी ऊर्जा और उसके विभिन्न तत्वों को संरक्षित करना है, और हमारे सहयोगी इन विचारों को सकारात्मक तरीके से पूरे भारत में आगे लेकर जाते हैं। संवाद का यही सार है। अब हमने 10 साल पूरे कर लिए हैं और दूसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय हम भविष्य की दिशा पर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले दशकों में संवाद की क्या भूमिका होनी चाहिए। यह साल इस प्रक्रिया को समझने और सुनने में बीतेगा, और फिर हम देखेंगे कि संवाद आगे किस दिशा में जाना चाहिए।
गाँव कनेक्शन: आपने भविष्य की बात की। इतने सालों में बहुत सारे चुनौतियाँ भी आई होंगी, बहुत कुछ सीखा भी होगा। आप संवाद का भविष्य कैसे देखते हैं?
सौरव रॉय: संवाद आदिवासियत का एक कार्यक्रम है, जो आदिवासी पहचान के विभिन्न तत्वों के इर्द-गिर्द घूमता है। हम इस पहचान को शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी विकासशील थीम के तहत नहीं देखते हैं, बल्कि इसे सिर्फ पहचान के लिए पहचान के रूप में समझते हैं। हमें समय के साथ तालमेल बैठाते हुए भविष्य के लिए तैयार रहना है। हमें यह भी देखना है कि हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ किस गति से आगे बढ़ना है। कुछ पहलुओं, जैसे भाषाओं और कला पर तेजी से काम करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन हर जगह एक ही गति नहीं हो सकती है। हमें यह देखना होगा कि किस दिशा में जाना है। साथ ही, इस मंच को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करनी है। भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें से अब तक 250 से अधिक जुड़ चुकी हैं। हमें इस संख्या को और बढ़ाना है ताकि अधिक आवाज़ें यहाँ तक पहुँचे। पिछले 10 सालों में 350 से अधिक छोटी-बड़ी बौद्धिक संपत्तियाँ निकली हैं, जिनमें भाषाओं की डिक्शनरी, किताबें, शिक्षण सामग्री, मौलिक संगीत रचनाएँ, पेंटिंग्स और कविताएँ शामिल हैं। इनकी संख्या बढ़ानी है ताकि हम मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित कर सकें। इस मूल चरित्र को बरकरार रखते हुए आगे की दिशा मिलती रहेगी।
गाँव कनेक्शन: आपने कहा कि 250 से ज्यादा जनजातियाँ संवाद से जुड़ी हुई हैं। ये जनजातियाँ अलग-अलग राज्यों और कोनों में रहती हैं। आप कैसे इन तक पहुँचते हैं और कैसे पहचानते हैं कि किसे संवाद में आना चाहिए?
सौरव रॉय: इसका श्रेय हमारी टीम को जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम संवाद को देखते हैं, यह हमारे लिए एक तरह का विकासशील स्कूल है। हमारी टीम संवाद के जरिये हर साल बहुत कुछ सीखती है। जितने लोग संवाद में शामिल होते हैं, उनसे हुई बातचीत हमें साल भर सीखने और इस अनुभव को समझने में मदद करती है। यह संवाद के कारण ही संभव हो पाता है। इसके अलावा, कई साथी जो पहले से संवाद का हिस्सा हैं, अब इसके एंबेसडर बन चुके हैं। उनका कहना होता है कि संवाद से जुड़ने से आपको दोस्त, पियर ग्रुप, संरक्षक और आत्मविश्वास मिलेगा। इससे काफी हद तक स्वाभाविक रूप से लोग जुड़ते हैं। इसके अलावा, हम और भी कई संस्थाओं से संपर्क करते हैं और नए-नए स्थानों पर जाकर नए मित्र बनाते हैं, आइडियाज़ साझा करते हैं। यही प्रक्रिया है जिससे हम नए-नए समुदायों तक पहुँचते हैं। कहीं यह प्रक्रिया आसान होती है और कहीं थोड़ी जटिल।

संवाद कॉन्क्लेव हर साल 15 नवंबर से 19 नवंबर तक होता है, लेकिन उसके पहले हमारा लीडरशिप प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम, रीजनल संवाद आदि पूरे साल चलते रहते हैं। इसमें हमारे साथियों से मुलाकात होती रहती है। हमारे ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम या संवाद फेलोशिप में ऐसे साथी हैं, जो 3-4 या 5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ दोस्ती और भरोसा बना है। हमने सीखा है कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। जैसे आप रीजनल संवाद आयोजित करिए, हमारी टीम से शायद एक ही सदस्य जाएगा, बाकी वहाँ की 8-10 लोगों की टीम वहीँ पर रीजनल प्रोग्राम संभाल लेगी।
अगर हम किसी राज्य में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आस-पास के राज्यों से लोग आकर उसे सफल बना देते हैं। यही बड़े लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। हमारी टीम बहुत एक्टिव और अपडेटेड रहती है, ताकि भारत को महीन तरीके से समझ सकें। हम भारत के ग्रासरूट नेटवर्क्स से जुड़े हुए हैं, यह नेटवर्क वाई-फाई की तरह काम करता है, और इसे समझना और इससे जुड़े रहना तकनीकी कौशल की बात है। हमारी टीम इस कला को जानती है, सीखती है, और इसे लागू करती है।
गाँव कनेक्शन: संवाद का मंच और जलवायु परिवर्तन किस तरह जुड़े हुए हैं ?
सौरव रॉय: मैं कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज केवल एक शब्द नहीं है, यह एक सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक पृथ्वी और सभी ग्रहों का सवाल है, आदिवासी समुदायों की जीवनशैली और उनकी प्राचीन बुद्धिमत्ता में इन जटिल प्रश्नों का उत्तर छिपा है, जिनका सामना हम सभी कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ये उत्तर हमारे सामने उन भाषाओं में नहीं हैं जो हम आमतौर पर समझ पाते हैं। ये पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन या अंग्रेजी में नहीं हैं, बल्कि गहरे संवाद में छिपे हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि धरती की धड़कन को कैसे समझा जाए। यह हमें संवाद से सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप यहां हैं, तो कभी-कभी एक गाने के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण संदेश हमें मिल सकता है, और उसे पकड़ना महत्वपूर्ण होता है।
दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में बहुत कुछ पहले से हो रहा है, और यह अच्छे स्तर पर हो रहा है। इसमें संसाधनों की इतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पर्याप्त संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं, और कभी-कभी इसके लिए पैसे की भी जरूरत नहीं होती। जो एक्शन हो रहा है, वह संवाद में कैप्चर होता है, और वह 80 सालों की अनुभवों में देखा जा सकता है।
जहाँ तक क्लाइमेट मिटीगेशन की बात है, हमारे नेटवर्क सबसे कमजोर क्षेत्रों तक पहुँच रखते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में केरल में बाढ़ आई थी, और जो प्रभावित क्षेत्र था, उसमें पहली प्रतिक्रिया हमारी TLP (ट्राइबल रिसर्च प्रोग्राम) टीम के साथियों से आई थी। कटे हुए क्षेत्र के दोनों ओर हमारी टीम थी, और उनकी वजह से पहला समन्वय संभव हो पाया।
इसके अलावा, कई जगह जहाँ बुराइयाँ और वल्गैरिटीज़ होती हैं, उनके बारे में बात करना, गाने लिखना, या जब कोई चक्रवात आता है, तो उन समुदायों को इससे कैसे निपटना है, यह संवाद के माध्यम से सिखाया जाता है। यह संवाद स्थिरता की वास्तविक भाषा है, और हमें इसे सही ढंग से समझना होगा। समाधान को समग्र दृष्टिकोण से देखना होगा। आप सात कदम इस दिशा में चल सकते हैं, पर तीन कदम उस दिशा में भी चलना जरूरी होगा, और ये तीन कदम इतने जटिल होते हैं कि वे सात कदमों से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ।”
गाँव कनेक्शन: आदिवासी हीलर्स को मंच देने को लेकर आपकी क्या योजना है?
सौरव रॉय: जी, हीलर्स का काम काफी जटिल था, खासकर कोविड के बाद। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रयास हो रहे हैं, जो स्वाभाविक और आवश्यक हैं। हम इन प्रयासों पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि यह सही दिशा में हो रहा है। अब जहाँ तक आदिवासी हीलर्स की बात है, हमारा प्रयास बहुत सरल है। खासकर कोविड के बाद, सार्वजनिक स्वास्थ्य और हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जो जरूरी भी हैं। लेकिन आदिवासी हीलर्स के लिए जो जगह है, उसमें हमें यह देखना है कि पारंपरिक चिकित्सा और एविडेंस बेस्ड चिकित्सा के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। हम कैसे यह प्रमाणित कर सकते हैं कि उनका इलाज भी प्रभावी है?

हमारा मानना है कि सबसे पहले इन्हें संगठित करना जरूरी है। इसलिए हमारा प्रयास यही है। आपने संवाद में देखा होगा कि हमारे लगभग 180 हीलर्स 18 राज्यों से जुड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सामूहिक समूह बने, ताकि उनकी जानकारी और ज्ञान प्रणाली का दस्तावेजीकरण हो सके, और यह अलग-थलग न रह जाए।
आदिवासी चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं, सदियों से यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन संवाद का मानना है कि हमें इसे एक दशक की इकाई के रूप में देखना चाहिए। हमें इसे स्थापित करने में 8-10 साल लग सकते हैं। अब हम इस प्रयास में लगे हैं कि एक सामूहिक संस्था बने, ताकि यह संगठित हो सके। पिछले तीन सालों में हमने यह देखा है कि हीलर्स अब एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, एक-दूसरे को पहचान रहे हैं। दक्षिण के आदिवासी हीलर्स उत्तर के हीलर्स को समझ रहे हैं, और एक-दूसरे के पास जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 वर्षों में हमें इस क्षेत्र में एक संगठित समूह देखने को मिलेगा।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि चिकित्सा में प्रमाण इकट्ठा करना आसान नहीं है, लेकिन अगर यह संगठित हो जाता है, तो यह एक मजबूत नींव बनेगी, जिसके आधार पर और भी प्रयास किए जा सकेंगे। संवाद का उद्देश्य इसी दिशा में एक मजबूत नींव तैयार करना है, खासकर आदिवासी चिकित्सा के क्षेत्र में।
गाँव कनेक्शन: अलग-अलग आदिवासी समुदाय को लेकर एक संगीत बैंड भी बनाया गया है, इसका विचार कैसे आया?
सौरव रॉय: रिदम्स ऑफ़ द अर्थ एक प्रयास है कि संगीत, वाद्य यंत्र, और गीतों का एक सामूहिक संग्रह बनाया जाए। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न आदिवासी समुदायों के संगीत, वाद्य यंत्रों और संगीतकारों को एक मंच पर लाना है। अगर हम आदिवासी संगीत की बात करें, तो इसका अधिकतर हिस्सा प्रदर्शन पर आधारित होता है। मंच पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं, और यह सही भी है। लेकिन आदिवासी समुदायों में सोच, शब्द, और सुर स्टूडियो के पहले के सभी महत्वपूर्ण घटक होते हैं, और यह सब एक साथ मिलकर संगीत का निर्माण करते हैं।
हमारा विचार यह है कि हम कैसे ऐसे लोगों का एक समूह बना सकते हैं, जिन्हें न केवल प्रदर्शन करने वाले संगीतकार के रूप में जाना जाए, बल्कि वे ऐसे संगीत निर्माता बनें जो आधुनिक संगीत के इस दौर में कुछ नया और मौलिक रचनाएँ करें। आज की ऑडियंस भी इस प्रक्रिया में शामिल हो रही है, और यहीं से ‘रिदम्स’ का विचार आया। संवाद में हम हमेशा विभिन्न और विविध लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ‘रिदम्स’ में भी यही किया जा रहा है।

अगर आप ‘रिदम्स’ के गाने सुनेंगे, तो आपको एक ही गाने में 3-4 अलग-अलग प्रकार के वाद्य यंत्र सुनाई देंगे। ये वाद्य यंत्र विभिन्न प्रकार के होंगे, और इसका निर्माण एक रेजीडेंसी मोड में होता है, जो 12 महीने तक चलता है। इस प्रक्रिया में पहले 12 महीनों तक संगीतकार एक-दूसरे से दोस्ती करते हैं, एक-दूसरे के जीवन और अनुभवों को समझते हैं। इसके बाद, वे यह चर्चा करते हैं कि किस विषय पर गाना लिखा जाए। फिर आवाजें निकल कर आती हैं, उसके बाद शब्द और सुर डाले जाते हैं, और अंत में उसे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाता है।
यह पूरी प्रक्रिया लगभग 12 महीने चलती है, और एल्बम का पहला लॉन्च संवाद में होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था साइक्लोन के बारे में, एक बेहतरीन गाना साइक्लोन पर आधारित है। इसमें एक पेड़ है जो झुक रहा है, और मेटाफर्स और अनुभव उस गाने में उभर कर आते हैं। यह अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, खासकर समकालीन समय में पारंपरिक आदिवासी भाषा में। यही ‘रिदम्स ऑफ़ द अर्थ’ करने की कोशिश कर रहा है, कि कैसे समकालीन समय की अभिव्यक्ति को पारंपरिक आदिवासी भाषा में लाया जाए।
गाँव कनेक्शन: संवाद में आकर आदिवासियों को क्या मिल रहा है ?
सौरव रॉय: संवाद में सबसे पहले एक ऐसा मंच बनाया जाता है, जहाँ आपसे यह नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए हैं। यहाँ किसी तरह का निर्णय या पूर्वाग्रह नहीं होता। हम इसे एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जहाँ आप अपनी शंकाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने संघर्षों या किसी भी अनुभव को बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आपको सुनने वाले लोग मिलते हैं, और इससे आत्मविश्वास मिलता है कि आप अपनी कहानी दूसरों के सामने रख सकते हैं। साथ ही, यहाँ आपको एक पियर ग्रुप मिलता है।
यह पियर ग्रुप कई उदाहरणों में मिलता है—सोचिए, झारखंड की कोई लड़की अरुणाचल, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश से दोस्त बना लेती है। ऐसे में उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये 4-5 अलग-अलग दोस्त एक साथ मिलकर कई प्रकार के स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ते हैं। आप समझते हैं कि चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हों, आपकी महत्वाकांक्षाएं एक समान होती हैं। आपको नए दोस्त मिलते हैं, एक तरह की एकता का अहसास होता है, और आपको मेंटॉरशिप भी मिलती है।
संवाद में ऐसे कई साथी होते हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत कुछ कर चुके होते हैं, जिन्हें हम दिग्गज कह सकते हैं, और वे ज्ञान से समृद्ध होते हैं। जब वे संवाद में आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं होती, बल्कि सीखने की प्रक्रिया अलग और सहज होती है। आप एकदम पीछे बैठकर आराम से काम कर सकते हैं, थोड़े पैनल डिस्कशन हो रहे होते हैं। यह सीखने का एक अनूठा तरीका है।
अक्सर लर्निंग प्रोसेस उन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो पहले से ही आत्मविश्वास से भरे होते हैं। लेकिन संवाद का प्रयास यह होता है कि हम ऐसे लर्निंग प्रोसेस तैयार करें जो उन लोगों को भी अपील करें, जो आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। यह संवाद का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और यही यहाँ हासिल किया जाता है।
जैसा मैं कह रहा था, संवाद एक ट्राइबल पहचान का मंच है। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी ट्राइबल आइडेंटिटी के एलिमेंट्स हो सकते हैं, उन पर काम किया जाए, चाहे वह भाषा हो, कला हो, संगीत हो, हीलिंग हो, खेल हो, आदि। हमने जब समाज से फीडबैक लिया, तो हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से यह समझ में आया कि सिनेमा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी कारण हमने समुदाय के साथ मिलकर इंडिजिनस सिनेमा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया।
हमने फिल्म प्रतियोगिताओं की शुरुआत की, और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक फिल्म निर्माताओं को जोड़ा जाए, जो ट्राइबल समुदायों से आते हैं। ये लोग सही दृष्टिकोण, सही एटीट्यूड, और सही समझ रखते हैं, ताकि वे खुद को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। अभी तक हमारे साथ लगभग 150 फिल्म निर्माता जुड़े हुए हैं, जो समुदाय के साथ काम कर रहे हैं। इसमें अनुभवी फिल्म निर्माता भी हैं और साथ ही नए उभरते हुए फिल्म निर्माता, फिल्म संपादक, निर्देशक, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिनेमा से प्रेरित अभिनेता हैं, जो सिनेमा को बहुत प्यार करते हैं।
गाँव कनेक्शन: मुख्यधारा की मीडिया ने आदिवासियों को रूढ़ियों में बाँध रखा है, इसे लेकर संवाद क्या कर रहा है?
सौरव रॉय: देखिए, इसका उत्तर बहुत सीधा है। यह हमारा निर्णय है और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, संवाद का उद्देश्य ट्राइबल पहचान के बारे में बात करना हो सकता है, लेकिन जिस दिन संवाद लोगों को यह बताने लगेगा कि उनकी पहचान क्या है, उस दिन हम बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। संवाद का उद्देश्य यह है कि लोग आएं और खुद खोजें कि वे क्या करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि संवाद एक ऐसा मंच है जहाँ कोई भी किसी को उनकी पसंद के लिए जज नहीं करता।
अगर आपकी विकास मॉडल की पसंद क्या है या आपका निर्णय क्या है, यह पूरी तरह से आपका होता है। संवाद का काम यह है कि लोगों को एक साथ लाकर नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को समझने का मौका देना। यह एक आईने की तरह है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं और दूसरों से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर पांच बूँदी जैसे समुदाय सही नीयत से आदिवासी समाज के बारे में सोचते और बात करते हैं, तो वे सही निर्णय भी लेते हैं। यह किसी अन्य समुदाय की तरह ही है।
संवाद का उद्देश्य कोई निर्णय थोपना या किसी प्रकार की सिफारिश करना नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ लोग अपने सवालों के साथ आते हैं और उन्हें खुद अपने उत्तर खोजने का अवसर मिलता है। कुछ सवालों के उत्तर आपको तुरंत मिल सकते हैं, जबकि कुछ उत्तर पाने में आपको चार साल का समय लग सकता है। यही संवाद की असलियत है।